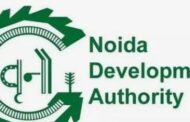लेखक-अरविंद जयतिलक
फिल्मों का एक सुनियोजित रणनीति के तहत विवादों में परोसना और फिर उस पर वितंडा खड़ा करके प्रचार पाना अब कोई नयी बात नहीं रह गई है। दरअसल फिल्मकारों ने आस्था, भावना और मूल्यों के खिलाफ फिल्में बनाकर बेशुमार धन इकठ्ठा करने का एक चलन बना लिया है। भले ही इससे किसी जाति, धर्म आस्था और भावना को चोट क्यों न पहुंचती हो। ऐसी ही एक फिल्म ‘घुसखोर पंडित’ भी रुपहले पर्दे पर चढ़ने को तैयार है जिसके टाईटल को लेकर वितंडा उठ खड़ा हुआ है। देश के विभिन्न हिस्सों में इस फिल्म के टाईटल को लेकर विरोध-प्रदर्शन जारी है। खुद फिल्म निर्माता संघ (एफएमसी) ने इस फिल्म को लेकर निर्माता नीरज पांडेय को नोटिस जारी किया है और कहा है कि फिल्म निर्माता ने नियमों के अनुसार शीर्षक के लिए अनिवार्य अनुमति प्राप्त नहीं की है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि फिल्म निर्माता ने जानबुझकर फिल्म को विवादों की परिधि में लाकर प्रचार पाने के लिए यह सारा उपक्रम किया था। अब जब विवाद चरम पर पहुंच गया है और फिल्म भी खूब प्रचार पा ली है तो फिल्म निर्माता नीरज पांडेय और अभिनेता मनोज वाजपेई द्वारा सफाई दी जा रही है कि उनका मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। वे अब विवादित प्रचार सामग्री को हटाने की भी दुहाई दे रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि फिल्म निर्माता ने अपनी फिल्म को विवादों के जरिए जितना प्रचार पाना चाहा था उतना पा लिया। उसका मकसद पूरा हुआ। अब सवाल यह है कि क्या ऐसे फिल्म निर्माताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी जो धन कमाने के निमित्त इस किस्म का घिनौने हथकंडा अपनाते हैं। कहना मुश्किल है। इसलिए कि इस तरह के हथकंडे बार-बार अपनाए जा रहे हैं। याद होगा गत वर्ष पहले ओम राउत निर्देशित फिल्म आदिपुरुष भी आई थी जिसमें अमर्यादित और फूहड़ संवादों और बेतुकी कल्पनाओं के जरिए भगवान श्रीराम और उनके भक्त हनुमान के अपमान के साथ-साथ महाकाव्य रामायण की प्रमाणिकता, ऐतिहासिकता, संदर्भ, गरिमा और आस्था से जमकर खिलवाड़ किया गया था। इसी तरह तमिल फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई ने अपनी फिल्म काली के पोस्टर में हिंदू देवी का रुप धरे महिला किरदार को सिगरेट पीते दिखाया था। इस किरदार के एक हाथ में एलजीबीटीक्यू समुदाय के 6 रंगे झंडे को भी दिखाया गया था। तब भी विरोध हुआ था लेकिन लीना मणिमेकलाई हिंदू संवेदनाओं को समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं दिखी। तब उन्होंने कहा था कि वह जीवित रहने तक निडर होकर अपनी आवाज का इस्तेमाल करती रहेंगी। विडंबना यह है कि तब भी कुछ सेलिब्रेटी राजनीतिक हस्तियां लीना मणिमेकलाई के समर्थन में आवाज बुलंद करती दिखी थी जैसा कि आज ‘घुसखोर पंडित’ टाईटल के समर्थन में खड़े दिख रहे हैं। मौंजू सवाल यह कि क्या नीरज पांडेय, ओम राउत और लीना मणिमेकलाई सरीखे फिल्म मेकर्स हिंदू जातियों, हिंदू धर्म, हिंदू आस्था की तरह अन्य धर्मों की जातियों, उनके आराध्यों और उन्हें असहज करने वाली भावनाओं को अपनी फिल्मों में अमर्यादित तरीके से दिखाने का साहस कर सकते हैं? शायद नहीं। तब फतवा जारी हो जाएगा और उन्हें जान बचाने के लाले पड़ जाएंगे। याद होगा गत वर्ष पहले देश के जाने-माने फिल्मकार संजय लीला भंसाली ने फिल्म ‘पद्मावती’ के जरिए रानी पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के बीच प्रेम संबंधों का निरुपण कर वितंडा खड़ा किया था। इसे लेकर देश में भारी बवाल हुआ था। मार्च 2015 में फिल्म ‘डर्टी पॉलिटिक्स’ भी विवादों से घिरी जब फिल्म का फर्स्टलुक जारी हुआ। इस पोस्टर में अभिनेत्री मल्लिका तीन रंगों वाले राष्ट्रीय ध्वजों में लिपटी नजर आयी। हैदराबाद उच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका पर मल्लिका और सरकार को नोटिस भी जारी किया। जनवरी 2016 में हंसल मेहता की फिल्म ‘अलीगढ़’ में समलैंगिक शब्द के इस्तेमाल पर सेंसर बोर्ड ने ऐतराज जताया। उल्लेखनीय है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्रीनिवास रामचंद्र सीरस के जीवन से जुड़ी सत्य घटना पर आधारित इस फिल्म में मनोज वाजपेयी और राजकुमार राव ने प्रमुख भूमिका निभायी थी। अभी गत वर्ष पहले अनुराग कश्यप निर्देशित फिल्म ‘उड़ता पंजाब’ विवादों के केंद्र में रहा। इस फिल्म का कथानक पंजाब में नशाखोरी के इर्द-गिर्द गढ़ा-बुना गया था। इसके कुछ दृश्यों और डॉयलाग को लेकर बवाल मचा। बेशक एक फिल्मकार को अधिकार है कि वह फिल्मों का निर्माण करे। लेकिन उसका उत्तरदायित्व भी है कि वह धर्म, संस्कृति और इतिहास को पढ़े-समझे और उसकी वास्तविकताओं एवं भावनाओं का ख्याल रखकर फिल्मों का निर्माण करे। उसे ध्यान रखना चाहिए कि फिल्मों के जरिए समाज के नैसर्गिक स्वभाव और आस्था पर बुरा असर न पड़े। यह उचित नहीं कि चंद पैसों के लालच में या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ लेकर हिंदू धर्म, संस्कृति और इतिहास पर हमला किया जाए। देखा जा रहा है कि विगत कई दशकों से भारत में हिंदू देवी-देवताओं और सनातन संस्कृति को टारगेट कर फिल्में बनायी जा रही हैं। यह सोच न सिर्फ विघटनकारी और नफरतपूर्ण है बल्कि भारतीय संस्कृति, सभ्यता, धर्म, संस्कृति और इतिहास पर प्रहार भी है। दरअसल इसके दो मकसद हैं। एक, हिंदू धर्म को बदनाम करना और दूसरा विवादों के जरिए अकूत संपदा इकठ्ठा करना। विश्वरुपम, हैदर, एमएसजी, पीके, मद्रास कैफे, सिंघम, आरक्षण, माई नेम इज खान, जोधा-अकबर, वाटर, जो बोले सो निहाल और फायर इत्यादि फिल्में इसी तरह का उदाहरण हैं। फिल्मकारों ने यह धारणा पाल रखी है कि फिल्मों पर जितना अधिक बवाल होगा उनकी कमाई में उतना ही इजाफा होगा। बेशक एक स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज में कहने-सुनने, लिखने-पढ़ने और दिखने-दिखाने की आजादी होनी चाहिए। विशेष रुप से कला के क्षेत्र में तो और भी अधिक। क्योंकि समाज में जो कुछ भी घटित होता है, उसे कला के जरिए पर्दे पर उकेरा जाता है। लेकिन कला और अभिव्यक्ति की आड़ लेकर अरबों कमाने की लालच में किसी धर्म और आस्था पर प्रहार कहां तक उचित है? एक वक्त था जब फिल्मों का कथानक समाज और राष्ट्र के जीवन में चेतना का संचार करता था। युवाओं को प्रेरणा देता था। आजादी की लड़ाई को धार देने से लेकर समाज के गुणसूत्र को बदलने-रचने में फिल्मों की अहम भूमिका रही है। आज भी कुछ फिल्में सामाजिक व राष्ट्रीय सरोकारों को उकेरती दिख जाती हैं। लेकिन अधिकांश फिल्में वास्तविकताओं से दूर अतिरंजित और फूहड़पन से लैस होती हैं। नतीजा उन्हें विवादों का विषय बनते देर नहीं लगती। इसमें किसी को आपत्ति नहीं कि फिल्मों का शीर्षक क्या हो अथवा उसका कथानक कैसा हो यह तय करने का अधिकार फिल्म के प्रोड्यूसर और निर्देशक का है। एक फिल्मकार को अधिकार और आजादी है कि वह ऐतिहासिक और धार्मिक कथानकों को फिल्मों के जरिए दुनिया के सामने लाए। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि वह धार्मिकता, ऐतिहासिकता और प्रमाणिकता के साथ छेड़छाड़ कर आस्था लहूलुहान करे। अगर किसी फिल्म के शीर्षक, कथानक या डॉयलाग से समाज का कोई वर्ग आहत होता है तो इसकी जिम्मेदारी सेंसर बोर्ड की है कि वह इसे पास न करे। याद होगा दिसंबर 2015 में ‘क्या कूल हैं हम’ और ‘मस्तीजादे’ पर सेंसर बोर्ड ने कैंची चलायी थी। ‘क्या कूल हैं हम’ में 107 सीन प्रोड्यूसर ने, जबकि 32 सीन सेंसर बोर्ड ने काटे थे। इसी तरह ‘मस्तीजादे’ में 349 सीन प्रोड्यूसर ने जबकि 32 सीन सेंसर बोर्ड ने काटे थे। इसके बाद भी इन फिल्मों को ‘ए’ सर्टिफिकेट के साथ रिलीज की अनुमति दी गयी। नवंबर 2015 में जेम्स बांड की सीरिज की 24 वीं फिल्म ‘स्पेक्टर’ के एक दृश्य पर भी सेंसर बोर्ड ने कैंची चलायी गयी थी। सवाल लाजिमी है कि फिर किसी फिल्म का नाम ‘घुसखोर पंडित’ कैसे रख दिया गया। इस अनुचित और अविवेकपूर्ण टाईटल पर कैंची क्यों नहीं चलायी गई? उचित होगा कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड अथवा भारतीय सेंसर बोर्ड फिल्मों के अनुचित टाईटल, दृश्यों और अनर्गल संवादों पर तत्काल कैंची चलाए ताकि देश-समाज का माहौल विषाक्त न बने और न ही किसी की भावना को ठेस पहुंचे।

(लेखक राजनीतिक व सामाजिक विश्लेषक हैं)