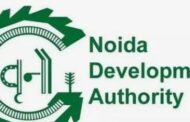लेखक:इब्न खल्दुन भारती
क्या भारतीय मुसलमानों में कोई बौद्धिक वर्ग है? यदि हां, तो फिर हिंदू वामपंथी-उदारवादियों को सार्वजनिक बहसों में उनका प्रतिनिधित्व क्यों करना पड़ता है? यदि मुसलमान अपना प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होते तो क्या उन्हें यह दान करना पड़ता? दुखद वास्तविकता यह है कि आसपास एक भी मुस्लिम बुद्धिजीवी नहीं है जो आधुनिक सार्वजनिक चर्चा के लिए आवश्यक क्षमता, कौशल और परिष्कार के साथ अपने समुदाय के मामले का प्रतिनिधित्व कर सके।
इसका कारण शिक्षा की कमी नहीं है. 75 प्रतिशत से अधिक साक्षरता दर के साथ, भारत में मुसलमानों के पास उच्च शिक्षित लोगों का एक बड़ा समूह है जो राष्ट्रीय हितों के मामलों में अन्य लोगों की तरह ही जोश और दृढ़ता के साथ हस्तक्षेप कर सकते हैं। लेकिन पत्रकार हामिद दलवई के शब्दों में, समस्या यह है कि ”मुस्लिम बुद्धिजीवी” शब्द के वास्तविक अर्थ में बुद्धिजीवी नहीं है। वह केवल एक मुसलमान है”। और चूँकि वह अपने धार्मिक व्यक्तित्व से थोड़ा अधिक है, इसलिए यह काफी स्वाभाविक है कि समुदाय का प्रतिनिधित्व क्षेत्र में बेहतर योग्य लोगों – मौलवियों – धर्म के पेशेवरों द्वारा किया जाता है। उनके प्रतिगामी अपमान जितने शर्मनाक हैं, क्या कोई आश्चर्य है कि टीवी पैनल चर्चाओं में अक्सर मौलवियों को क्यों देखा जाता है, न कि आधुनिक मुसलमानों को? दलवई किसी समाज की प्रगति को उसके बौद्धिक वर्ग की स्थापित परंपराओं और समाज की सामान्य समझ को तर्कसंगत जांच के अधीन करने की क्षमता, लोगों की संवाद और द्वंद्वात्मकता की भावना से ऐसी आलोचना से जुड़ने की क्षमता और समायोजन द्वारा मापते हैं। असहमति और असंतुष्ट. “हालांकि, बुद्धिजीवियों का ऐसा वर्ग इतनी आसानी से अस्तित्व में नहीं आता है। यह कई जटिल ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य प्रक्रियाओं का उत्पाद है।
भारत में मुस्लिम समुदाय परिवर्तन की ऐसी प्रक्रिया से नहीं गुजरा है।” और इसलिए, जैसे ही कोई मुसलमान मुस्लिम समाज की ओर आलोचनात्मक दृष्टि डालता है, विशेष रूप से इसके इतिहास और राजनीति पर, यानी भारत में उनके लंबे शासन और अलगाववाद की राजनीति पर, वे रद्द और बहिष्कृत हो जाते हैं। दलवई का भी यही हश्र हुआ। दो सर्वाधिक निंदित शख्सियतें 1960 से 80 के दशक तक, उर्दू प्रेस में सबसे अधिक निंदित व्यक्ति दो साथी मुस्लिम थे, अर्थात् एमसी छागला, जो बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के शिक्षा मंत्री थे; और हामिद दलवई. उनकी पुस्तक, मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया, जो पहले 1968 और 1972 में प्रकाशित हुई थी, को हाल ही में पेंगुइन द्वारा पुनः प्रकाशित किया गया है।
दलवई की पुस्तक में कहीं भी इस्लाम को एक धर्म के रूप में वर्णित नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि यह अलगाववादी राजनीति का एक माध्यम और रूढ़िवादी तथा मानवतावाद-विरोधी लक्ष्यों को प्राप्त करने का साधन है। वह केवल इस्लाम के गैर-धार्मिक या वैचारिक पक्ष में रुचि रखते थे और उन्होंने कभी भी धर्म के बारे में दूर-दूर तक आलोचनात्मक शब्द नहीं कहा या इसके सिद्धांतों और प्रथाओं पर सवाल नहीं उठाया। फिर मुस्लिम मत-निर्माता वर्ग उन्हें इस्लाम का दुश्मन क्यों मानने लगा? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे दलवई के विचारों की विध्वंसक क्षमता को पहचान गए थे।
अलगाववाद की उनकी सिद्धांतहीन राजनीति पर सवाल उठाकर, वह उनके 800 वर्षों के शासन की विरासत, उनके निरंतर अधिकारों और सत्ता पर दावे को कमजोर कर रहे थे, जिसे धर्मनिरपेक्षता के मुहावरे में दोहराया गया था। यह वर्ग धर्म में विधर्म को स्वीकार कर सकता है, लेकिन उनके राजनीतिक विशेषाधिकार पर सवाल उठाना अक्षम्य धर्मत्याग है। दलवई के प्रति मुस्लिम शत्रुता यह एहसास कराती है कि उनके लिए, इस्लाम, महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं है; वास्तव में जो महत्वपूर्ण है वह है उनकी राजनीति और शासन करने का अधिकार। इस्लाम केवल उसी हद तक महत्वपूर्ण हो जाता है जिस हद तक वह उनकी राजनीति को
सुविधाजनक बनाता है, जो वह पूरी तरह से करता है। सर सैयद अहमद खान के धार्मिक विचार मुसलमानों के लिए इतने अस्वीकार्य हैं कि उनकी अपनी संस्था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, कुरान पर उनकी टिप्पणी प्रकाशित करने से इनकार कर देती है। लेकिन, सर सैयद एक श्रद्धेय व्यक्ति हैं, क्योंकि वह हिंदुओं के राजनीतिक विकास के खिलाफ खड़े हुए और उन्होंने कॉलेज का निर्माण किया, जिसने मुसलमानों को उनके खिलाफ आधुनिक राजनीति का खेल खेलने के लिए तैयार किया। यदि उन्होंने अपने कौम को यह नहीं सिखाया होता कि आरंभिक राष्ट्रीय आंदोलन को अपनी स्थिति के लिए खतरा कैसे माना जाए, तो उनके धार्मिक विचारों ने उन्हें अहमदिया संप्रदाय के संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तुलना में अधिक बदनाम व्यक्ति बना दिया होता। इसी तरह, मुहम्मद अली जिन्ना इतने अधार्मिक थे कि उन्हें मुसलमानों की सबसे बड़ी वर्जना – सूअर का मांस खाने – को तोड़ने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी।
लेकिन वह उनके कायदे आज़म बन गए क्योंकि उन्होंने उनकी अलगाववादी राजनीति को सफल नेतृत्व प्रदान किया। इसके विपरीत, यदि वह सबसे महान संत होते, लेकिन उस राजनीति का विरोध करते, तो वह मुस्लिम समुदाय से सबसे खराब बदनामी से बच नहीं पाते। यह लेखक, लंबे समय से राजनीतिक इस्लाम की मावदुडियन थीसिस का विरोध कर रहा है, जो धर्म की व्याख्या इस तरह से करता है कि इसे एक राजनीतिक विचारधारा बना दिया जाए, और, इसलिए, मुसलमानों के लिए दुनिया पर शासन करने के लिए एक चार्टर, हाल ही में उसी की ओर बढ़ रहा है समझ, यद्यपि विपरीत दिशा से। इस्लाम का धर्मशास्त्र और धार्मिकता निस्संदेह सर्वोच्चता की ओर उन्मुख है।
दलवई के अनुसार, परिपूर्ण और अपरिवर्तनीय कानूनों के धर्म से संबंधित होने के अहंकार से उत्पन्न यह वर्चस्ववाद मुसलमानों के बीच सुधार की असंभवता और आलोचनात्मक विचारकों का एक वर्ग बनाने में उनकी असमर्थता की वैचारिक जड़ है। कहाँ हैं मुस्लिम विचारक? जब कोई भारतीय मुसलमानों के बीच आलोचनात्मक विचारकों के बारे में सोचता है, तो उसे सर सैयद के अलावा किसी अन्य नाम के बारे में सोचना मुश्किल हो जाता है। एक समाज सुधारक के रूप में उनकी लोकप्रिय छवि के बावजूद, सर सैयद ने मुस्लिम समाज की बुराइयों के लिए आलोचना नहीं की। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, एक सुधारक होने के बजाय, उन्होंने मुस्लिम शासक वर्ग के जन्मजात अलगाववाद का सिद्धांत दिया। हालाँकि, धर्मशास्त्र में, उन्होंने सुधारवाद की एक कट्टरपंथी भावना दिखाई। लेकिन उसका उद्देश्य भी आत्मज्ञान कम और मुसलमानों को अपनी सत्ता की स्थिति बनाए रखने के लिए बौद्धिक रूप से सक्षम बनाना अधिक था। हालाँकि अल्लामा इक़बाल को एक आलोचनात्मक विचारक कहना एक लंबी बात होगी, क्योंकि उनके प्रशंसक उन्हें एक कवि-दार्शनिक के रूप में पहचानते हैं, यह ध्यान रखना उचित है कि उन्होंने उलेमाओं को तिरस्कारपूर्वक “मुल्ला” कहकर उनके प्रति तिरस्कार को सामान्य बना दिया। उन्होंने मुस्लिम शासन के पतन का कारण होने के लिए उन्हें और इस्लाम के उनके संस्करण को दोषी ठहराया।
उनकी परंपरा के अनुरूप, आज के “आधुनिक-प्रगतिशील-उदारवादी मुसलमान” भी लगभग इसी कारण से उलेमा और उनके पुरातन धर्मशास्त्र के आलोचक हैं। दिखावे के विपरीत, वे उदार-धर्मनिरपेक्ष-राष्ट्रवादी नहीं हैं, बल्कि सांप्रदायिक-पहचानवादी-अलगाववादी हैं जो मुसलमानों को फिर से दुनिया पर हावी होने में सक्षम बनाने के लिए इस्लाम की आधुनिक व्याख्या का प्रयास करते हैं। मकसद बिल्कुल सर सैयद अहमद या अल्लामा इकबाल जैसा ही है। दलवई के अलावा, मुसलमानों के बीच किसी सच्चे बुद्धिजीवी या आलोचनात्मक विचारक का नाम बताना कठिन है।
उनकी मुख्य चिंता मुसलमानों का धर्मनिरपेक्षीकरण और उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करना था। उन्होंने मुसलमानों को एक समानांतर और स्वायत्त समाज – एक राज्य के भीतर एक राज्य और एक समाज के भीतर एक समाज – के रूप में बनाए रखने के लिए सर्वोच्चतावादी धर्मशास्त्र को दोषी ठहराया। उन्होंने यह जाने बिना कि मुस्लिम आधुनिकतावाद, जैसा कि अलीगढ़ आंदोलन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, शुरू से ही एक त्रुटिपूर्ण परियोजना थी, आधुनिकीकरण पर अपनी आशाएँ रखीं। यह राजनीतिक था, बौद्धिक नहीं, जिसका उद्देश्य ज्ञानोदय के बजाय पुनः सशक्तीकरण था।
धर्मनिरपेक्षीकरण के बजाय, इसने साम्प्रदायिकीकरण को बढ़ावा दिया। मुसलमानों का आधुनिकीकरण, उनकी चेतना के राष्ट्रीयकरण के बिना, संघर्ष का एक नुस्खा था, क्योंकि जहां भी वे अल्पसंख्यक हैं, उनमें राष्ट्रवाद के प्रति घृणा है। भारत में, अपने धार्मिक उप-राष्ट्रवाद को भारत की विशाल सभ्यतागत और क्षेत्रीय राष्ट्रवाद के साथ संश्लेषित करके इस पर काबू पाने की आवश्यकता है। यह संभव नहीं हो सका क्योंकि मुसलमानों ने इस कार्य के बराबर बौद्धिक वर्ग विकसित नहीं किया था। जहां भारतीय मुसलमान असफल रहे हैं मुसलमानों की सबसे बड़ी विफलता यह है कि वे अपना खुद का गांधी पैदा करने में असमर्थ रहे जो परंपरा को आधुनिकता के साथ, धार्मिक नैतिकता को राजनीतिक नैतिकता के साथ, सांप्रदायिक पहचान को राष्ट्रीय व्यक्तित्व के साथ और राष्ट्रवाद को सर्वदेशीयता के साथ जोड़ते थे। दलवई ने मुस्लिम गांधी के उद्भव को तब तक नहीं देखा जब तक “आधुनिक मूल्यों के प्रकाश में मुसलमानों के धर्म और संस्कृति की निर्मम जांच के अधीन लोगों की एक पीढ़ी द्वारा जमीन तैयार नहीं की जाती”।
बुद्धिजीवियों की अनुपस्थिति, और उनके द्वारा बनाई गई आलोचनात्मक संस्कृति, सबसे अच्छी तरह से प्रतिबिंबित होती है जिसे दलवाई “मुसलमानों का उत्पीड़न उन्माद” कहते हैं। वे अपनी सभी समस्याओं के लिए हिंदुओं को दोषी ठहराते हैं और अपनी स्थिति के लिए किसी भी जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे बौद्धिक पक्षाघात से पीड़ित हैं और अपनी असंतोषजनक स्थिति के पीछे के कारणों की आलोचनात्मक जांच करने में असमर्थ हैं। बंद व्हाट्सएप समूहों में, उनकी बातचीत पीड़ित सिंड्रोम से भरी होती है। यह एक लत और एक मनोवैज्ञानिक विकार है। दलवई एक तीखा सवाल पूछते हैं: आधुनिक शिक्षा के प्रति मुस्लिम प्रतिरोध के लिए हिंदू कैसे जिम्मेदार थे? उन्होंने हिंदू-मुस्लिम संबंधों पर दो चौंकाने वाली अंतर्दृष्टि भी पेश की, उन्होंने कहा कि मुस्लिम सांप्रदायिकता वैचारिक है जबकि हिंदू सांप्रदायिकता मुस्लिम आक्रामकता की प्रतिक्रिया है।
पहला इस्लामी विश्वास से उत्पन्न होता है कि हिंदू धर्म एक झूठा धर्म है और हिंदू गलत रास्ते पर हैं और मुसलमानों को उन्हें वश में करके और धर्मांतरित करके सही रास्ते पर लाना चाहिए। इसके विपरीत, हिंदू इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि किसी की आस्था क्या है। उन्हें सिर्फ इस बात की चिंता है कि मुसलमान उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं. तर्क को आगे बढ़ाते हुए, दलवई एक समझदार बात कहते हैं, “मेरा मानना है कि यदि हिंदू पर्याप्त रूप से गतिशील होते, तो हिंदू-मुस्लिम समस्या हल हो जाती। क्योंकि यदि हिंदू गतिशील होते, तो वे मुसलमानों को कई ऐसे झटके झेलते, जिनसे इतिहास उन्हें बचाता रहा है। अगर मुसलमान बदलना नहीं चाहते तो उनके पास ख़त्म होने का एक ही विकल्प बचेगा। और एक समाज विलुप्त होने की बजाय बदलाव को प्राथमिकता देता है।” क्या नरेंद्र मोदी उस इच्छा का उत्तर हैं? क्या वह लंबे समय से प्रतीक्षित सुधारक हैं जिनकी मुसलमानों को हमेशा आवश्यकता थी लेकिन वे पैदा नहीं कर सके? मोदी के प्रभाव में, मुसलमान वही बन गए हैं जिसका वे दावा करते हैं – शांतिपूर्ण! इससे पहले उन्होंने कभी भी ऐसी शांति का आनंद नहीं लिया था और इतने शांतिपूर्ण नहीं थे।
कोई आतंकी हमला नहीं. कोई दंगा नहीं. अयोध्या फैसले, समान नागरिक संहिता, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर एक परिपक्व प्रतिक्रिया। मुस्लिम कभी भी आत्मनिरीक्षण और सुधार के लिए इतने इच्छुक नहीं रहे हैं, और पहले कभी भी वे इतने प्रदर्शनकारी राष्ट्रवादी नहीं रहे हैं। सचमुच, मोदी है तो मुमकिन है। इब्न खल्दुन भारती इस्लाम के छात्र हैं और इस्लामी इतिहास को भारतीय नजरिए से देखते हैं।
(हुमरा लईक द्वारा संपादित और द प्रिंट में उल्लेखित विमर्श)