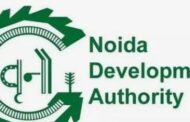लेखक-अरविंद जयतिलक
-गत दिवस अमेरिका के वाशिंगटन राज्य के केलर में रहने वाली पाॅलिन स्टेन्सगर का निधन इसलिए खूब सुर्खियों में रहा कि वह ‘इन-हा-उस-चीन’ देशज भाषा बोलने वाली वह अंतिम व्यक्ति थी। उनके निधन के साथ ही अब ‘इन-हा-उस-चीन’ भाषा का अस्तित्व भी खत्म हो गया। याद होगा गत वर्ष पहले मैक्सिकों की पुरानतम देशज भाषाओं में से एक अयापनेको के विलुप्त होने की खबरें भी खूब चर्चा में रहा। आज की तारीख में इस भाषा को जानने और बोलने वाले लोगों की संख्या महज दो रह गयी है। इन दो लोगों ने भी ठान लिया है कि वे आपस में इस भाषा के जरिए वार्तालाप नहीं करेंगे। मतलब साफ है कि अब अयापनेको भाषा का अस्तित्व भी मिटने जा रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक हर दो सप्ताह में एक देशज भाषा का अस्तित्व मिट रहा है। दुनियाभर में तकरीबन 6900 देशज भाषाएं बोली जाती है जिनमें से लगभग 2500 से अधिक भाषाओं के अस्तित्व पर संकट है। इन्हें ‘भाषाओं की चिंताजनक स्थिति वाली भाषाओं की सूची’ में रखने के लिए मजबूर होना पड़ा है। गत वर्ष पहले संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कराए गए एक तुलनात्मक अध्ययन से खुलासा हुआ कि 2001 में विलुप्तप्रायः देशज भाषाओं की संख्या जो 900 के आसपास थी वह बढ़कर तीन गुने से पार जा पहुंची है। दुनियाभर में तकरीबन 199 भाषाएं ऐसी हैं जिनके बोलने-लिखने वाले लोगों की संख्या एक दर्जन से भी कम है। उदाहरण के लिए उक्रेन में बोली जाने वाली कैरेम भी इन्हीं भाषाओं में से एक है जिसे बोलने वालों की संख्या महज 6 है। ओकलाहामा में विचिता भाषा बोलने वालों की संख्या 10 और इंडोनेशिया में लेंगिलू बोलने वालों की संख्या सिर्फ 4 है। विश्व में 178 देशज भाषाएं ऐसी हैं जिन्हें बोलने वाले लोगों की संख्या डेढ़ सैकड़ा है। किंतु दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि इन देशज भाषाओं को बचाने का अभी तक कोई ठोस पहल नहीं हुआ है। या यों कहें कि विलुप्त हो रही देशज भाषाओं को बचाने की दिशा में जितना सार्थक प्रयास होना चाहिए उतन नहीं हो रहा है। भाषायी वैज्ञानिकों की मानें तो इन देशज भाषाओं को बचाकर ही उनसे जुड़ी संस्कृति और उनकी ज्ञान परंपरा की रक्षा हो सकती है। भारत की बात करें तो यहां भी देशज भाषाओं के अस्तित्व पर संकट है। गत वर्ष पहले पीपल्स लिविंग्वस्टिक सर्वे आॅफ इंडिया (पीएलएसआइ) के जरिए यह खुलासा हुआ कि देश में बोली जाने वाली आठ सैकड़ा भाषाओं में आधी भाषाएं आगामी 50 वर्ष बाद सुनाई नहीं देंगी। देश में तकरीबन 780 भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें से 400 भाषाओं पर विलुप्ति का खतरा है। पिछले पांच दशकों में 250 भाषाएं विलुप्त हुई हैं। इनमें से 22 आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं भी हैं। गत वर्ष पहले ‘भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर’ द्वारा प्रकाशित अपने सर्वेक्षण में कहा गया कि देश में बोली जाने वाली 250 भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं। 130 से अधिक भाषाएं विलुप्ति की कगार पर हैं। इस शोध की मानें तो असम की 55, मेघालय की 31, मणिपुर की 28, नागालैंड की 17, और त्रिपुरा की 10 भाषाओं पर विलुप्ति का खतरा मंडरा रहा हैं। इन्हें बोलने वालों की संख्या लगातार तेजी से घट रही है। उदाहरण के तौर पर सिक्किम में माझी बोलने वालों की संख्या सिर्फ 4 रह गयी है। कमोवेश ऐसी ही स्थिति देश के अन्य देशज भाषाओं की भी है। जिन देशज भाषाओं के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है उनमें ज्यादतर आदिवासी समुदायों की भाषाएं हैं। उदाहरण के तौर पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल में ही 90 से अधिक देशज भाषाएं बोली जाती है। इनमें से कई देशज भाषाओं को बोलने वालों की तादाद ऊंगलियों पर है। ओडिसा में 47 और महाराष्ट्र एवं गुजरात में 50 से अधिक देशज भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन इनमें से कई देशज भाषाएं अब नाम भर की हैं। दरअसल इसका मूल कारण यह है कि आदिवासी समुदायों की बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा नहीं मिल रही है। वे स्कूल जाते हैं तो इन्हें 22 आधिकारिक भाषाओं में ही शिक्षा लेनी पड़ती है। उचित होगा कि इन बच्चों को उनकी देशज भाषाओं में भी शिक्षा की व्यवस्था हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो न सिर्फ दुनिया की बल्कि भारत की भी देशज भाषाएं खत्म हो जाएंगी। ध्यान देना होगा कि जिन भाषाओं के अस्तित्व पर सबसे ज्यादा संकट मंडरा रहा है वह सर्वाधिक रुप से उन जनजाति समूहों के बीच बोली जाती हैं जो आज की तारीख में कई तरह के संकट से गुजर रहे हैं। सबसे बड़ा संकट इनके जीवन की सुरक्षा को लेकर है। अमेरिका हो या भारत हर जगह विकास के नाम पर जंगलों का उजाड़ा जा़ रहा है। अपनी सुरक्षा और रोजी-रोजगार के लिए जनजातिय समूह के लोग अपने मूलस्थान से पलायन कर रहे हैं। दूसरे समूहों में जाने और रहने के कारण उनकी भाषा प्रभावित हो रही है। यही नहीं उन्हें मजबूरन दूसरी भाषाओं को अपनाना पड़ रहा है। इसके अलावा रोजी-रोजगार का संकट, बाहरी हस्तक्षेप और धर्म परिवर्तन इत्यादि भी कई ऐसे कारण है जिनकी वजह से इनकी कालजयी संस्कृति और भाषा समाप्त हो रही है। सत्य यह भी है कि दुनिया भर में अंग्रेजी भाषा के पसरते पांव और मिल रहे संरक्षण ने विश्व में बोली जाने वाली उन सैकड़ों लोक भाषाओं के अस्तित्व पर संकट खड़ा किया है। लेकिन इसके लिए अंग्रेजी भाषा को दोष नहीं दिया जा सकता। यह सही है कि विश्व में अंग्रेजी भाषा का बढ़ता प्रभाव और उसका रोजगार से जुड़ा होना अन्य लोकभाषाओं के अस्तित्व के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन यह अस्वाभाविक इसलिए नहीं है कि जब भी कोई भाषा रोजगार देने में सहायक सिद्ध होती तो उसे बोलने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही है। और जो भाषाएं रोजगार देने में नाकाम सिद्ध होती हैं वे उसकी कीमत विलुप्त होकर चुकाती हैं। अगर अंग्रेजी भाषा अन्य स्थानीय भाषाओं के विलुप्ती का कारण बन रही है तो इस बात पर विचार होना ही चाहिए कि क्यों न क्षेत्रीय भाषाओं को अंग्रेजी भाषा की तरह ही रोजगार परक बनाया जाए। यह एक तथ्य है कि विश्व के अधिकाश हिस्सों में बोली जाने वाली अंग्रेजी भाषा न सिर्फ अंतरर्राष्ट्रीय भाषा का रुप धारण कर चुकी है बल्कि बड़े पैमाने पर रोजगार भी उपलब्ध करा रही है। इन परिस्थितियों के बीच अगर अंग्रेजी भाषा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता है और स्थानीय भाषाएं दम तोडेंगी ही। क्षेत्रीय भाषाओं के विलुप्त होने के और भी बहुतेरे कारण हो सकते हैं जिनकी पड़ताल होनी चाहिए। यहां ध्यान रखना होगा कि विलुप्त हो रही भाषाओं को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की ही नहीं है। स्वयंसेवी व सामाजिक संस्थाओं को भी आगे आना होगा। ये भाषाएं तभी बचेंगी जब उन्हें संवैधानिक संरक्षण के साथ-साथ इन्हें रोजगार से जोड़ा जाएगा। अगर इन भाषाओं को सिर्फ शब्दकोषों तक सीमित रखने का प्रयास हुआ तो फिर इन्हें इतिहास के गर्त में जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। अच्छी बात यह है कि पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे आॅफ इंडिया दुनिया भर में बोली जाने वाली छः हजार से अधिक भाषाओं पर अध्ययन करने जा रही है जिसकी रिपोर्ट 2025 में प्रकाशित होगी। अच्छी बात है कि संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर की ऐसी देशज भाषाओं को विलुप्ति से बचाने के लिए अंतरराष्ट्रीय देशज भाषा दशक की पहल शुरु कर दी है। यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है कि देशज भाषाओं के संरक्षण से उनसे जुड़ी संस्कृति, परंपरा और ज्ञान का संरक्षण हो सकेगा। अगर इन्हें बचाने का ठोस पहल नहीं हुआ तो इन भाषाओं में से आधे से अधिक इस शताब्दी के अंत तक विलुप्त हो जाएंगी। देशज भाषाओं के अस्त्वि पर मंडराते संकट का असर जैव विविधता पर भी पड़ रहा है। भाषा विद्वानों की मानें तो अगर हम प्रकृति को बचाना चाहते हैं तो इसके लिए देशज लोगों की भाषाओं को समझना-जानना और बचाना बेहद जरुरी है। इसलिए कि दुनिया में जो भी जैव विविधता बची है उसका लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा इन्हीं लोगों ने बचाकर रखा।

-लेखक राजनीतिक व सामाजिक विश्लेषक हैं-