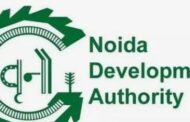लेखक-अरविंद जयतिलक
आज विश्व पर्यावरण दिवस है। यह दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक व सामाजिक जागृति लाने हेतु वर्ष 1972 में की थी। पर विडंबना यह है कि इस दिवस पर हम एक ओर पर्यावरण सुरक्षा के प्रति चिंता जाहिर करते हैं, संगोष्ठियां करते हैं, नए कानून गढ़ते हैं वहीं दूसरी ओर अंधाधुंध विकास के नाम पर प्रति वर्ष 7 करोड़ हेक्टेयर वनों का विनाश करते हैं। ऐसे में पर्यावरण दिवस मनाना अपने आप में बेमानी हो जाता है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले सैकड़ों सालों में मनुष्य जाति ने विकास के नाम पर करोड़ों हेक्टेयर वनों का विनाश किया हैै। उसके इस कृत्य से प्रकृति की तकरीबन एक तिहाई से अधिक प्रजातियां नष्ट हुई हैं। जंगली जीवों की संख्या में 50 फीसद की कमी आयी है। उदाहरण के लिए भारत में पिछले एक दशक में पर्यावरण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले गिद्धों की संख्या में 97 फीसद की गिरावट दर्ज की गयी है। इससे मृत पशुओं की सफाई, बीजों का प्रकीर्णन और परागण कार्य काफी हद तक प्रभावित हुआ है। गिद्धों की तरह अन्य प्रजातियां भी तेजी से विलुप्त हो रही हैं। वनों के विनाश से वातारण भी जहरीला होता जा रहा है। यानी प्रतिवर्ष 2 अरब टन अतिरिक्त कार्बन-डाइआक्साइड वायुमण्डल में घुल-मिल रहा है। इससे जीवन का सुरक्षा कवच मानी जाने वाली ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा है। नेचर जिओसाइंस की मानें तो ओजोन परत को होने वाले नुकसान से कुछ खास किस्म के अत्यंत अल्प जीवी तत्वों (वीएसएलएस) की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है जो मानव जाति के अस्तित्व के लिए खतरनाक है। विडंबना यह कि ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के मांट्रियाल प्रोटाकाल में इन तत्वों पर नियंत्रण की कोई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यदि इनमें लगातार इजाफा हो रहा है तो ओजोन परत के लिए नुकसानदायक स्वाभाविक है। गौरतलब है कि दुनिया के 20 सबसे ज्यादा क्लोरोफ्लोरो कार्बन उत्सर्जित करने वाले देशों के बीच ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए 16 सितंबर, 1987 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संधि हुई जिसे मांट्रियाल प्रोटाकॉल नाम दिया गया। इसका मकसद ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार गैसों एवं तत्वों के इस्तेमाल पर रोक लगाना था। लेकिन इस दिशा में अभी तक अपेक्षित सफलता हासिल नहीं हुई है। एक आंकड़ें के मुताबिक अब तक वायुमण्डल में 36 लाख टन कार्बन डाइआक्साइड की वृद्धि हो चुकी है और वायुमण्डल से 24 लाख टन आक्सीजन समाप्त हो चुकी है। अगर यही स्थिति रही तो 2050 तक पृथ्वी के तापक्रम में लगभग 4 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का तापमान जिस तेजी से बढ़ रहा है अगर उस पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो अगली सदी में तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। आज जब 48 डिग्री सेल्सियस की गर्मी मनुष्य के लिए असहनीय है तो 60 डिग्री सेल्सियस गर्मी को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तापमान बढ़ने से सूर्य की किरणें कैंसर जैसे भयंकर रोगों में वृद्धि करेगी। कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं गरम हवाएं चलेंगी तो कहीं भीषण तूफान व बाढ़ का सामना करना पड़ेगा। यदि पृथ्वी के तापमान में मात्र 3.6 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो जाए तो आर्कटिक एवं अण्टाकर्टिका के विशाल हिमखण्ड पिघल जाएंगे जिससे समुद्र के जल स्तर में 10 इंच से 5 फुट तक वृद्धि हो सकती है। इसका परिणाम यह होगा कि समुद्रतटीय नगर समुद्र में डूब जाएंगे। भारत के मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, पणजी, विशाखापट्टनम कोचीन और त्रिवेंद्रम नगर समुद्र में होंगे। इसी तरह न्यूयॉर्क, लॉस एंजिल्स, पेरिस और लंदन आदि बड़े नगर भी जलमग्न हो जाएंगे। याद दिला दें कि 5 जून 2007 में पर्यावरण दिवस का सबसे ज्वलंत विषय ‘पिघलती बर्फ’ था। इस पर मुख्य अंतर्राष्ट्रीय आयोजन नॉर्वे के ट्रामसे में संपन्न हुआ और दुनिया भर में ‘ग्लोबल आउटलुक फॅार आइस एंड स्नो’ की शुरुआत हुई। गौर करें तो पर्यावरण के साथ खिलवाड़ का सबसे घातक असर ध्रवीय क्षेत्रों पर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय अनुपात को देखते हुए उत्तरी ध्रुव क्षेत्र दोहरी तेजी से गरम हो रहा है। उत्तरी ध्रुव समुद्र में फैली स्थायी बर्फ की मोटी परत कम हो रही है। सदियों से बर्फ के मजबूत चादर में ढके क्षेत्र पिघल रहे हैं। वर्ष 2007 की इंटरगवर्नमेंटल पैनल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के करीब 30 पर्वतीय ग्लेशियरों की मोटाई वर्ष 2005 में आधे मीटर से ज्यादा कम हो गयी। वैज्ञानिकों को मानना है कि इसके लिए मुख्य रुप से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन जिम्मेदार है। हिमालय क्षेत्र में पिछले पांच दशकों में माउंट एवरेस्ट के ग्लेशियर 2 से 5 किलोमीटर सिकुड़ गए हैं। इसके अलावा हिमालय के 76 फीसद ग्लेशियर चिंताजनक गति से सिकुड़ रहे हैं। कश्मीर और नेपाल के बीच गंगोत्री ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ते ग्लेशियर का एक अन्य उदाहरण है। अनुमानित भूमंडलीय तापन से जीवों का भौगोलिक वितरण भी प्रभावित हो सकता है। कई जातियां धीरे-धीरे ध्रुवीय दिशा या उच्च पर्वतों की ओर विस्थापित हो जाएंगी। जातियों के वितरण में इन परिवर्तनों का जाति विविधता तथा पारिस्थितिकी अभिक्रियाओं इत्यादि पर असर पड़ेगा। पृथ्वी पर करीब 12 करोड़ वर्षों तक राज करने वाले डायनासोर नामक दैत्याकार जीवों के समाप्त होने का कारण संभवतः ग्रीन हाउस प्रभाव ही था। निश्चित रुप से मनुष्य के विकास के लिए प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का दोहन आवश्यक है। पर उसकी सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए। लेकिन उसका पालन नहीं हो रहा है। विकास के लिए बिजली आवश्यक है। लेकिन जिस तरह बिजली के उत्पादन के लिए नदियों के सतत प्रवाह को रोककर बांध बनाया जा रहा है उससे खतरनाक पारिस्थितिकीय संकट उत्पन हो गया है। जल का दोहन स्रोत सालाना रिचार्ज से कई गुना बढ़ गया है। पेयजल और कृषिजल का संकट गहराने लगा है। भारत की गंगा और यमुना जैसी अनगिनत नदियां सूखने के कगार पर हैं। वह प्रदुषण से कराह रही हैं। सीवर का गंदा पानी और औद्योगिक कचरा बहाने के कारण क्रोमियम और मरकरी जैसे घातक रसायनों से नदियों का पानी जहर बनता जा रहा है। वैज्ञानिकों की मानें तो जल संरक्षण और प्रदूषण पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले 200 सालों में भूजल स्रोत सूख जाएगा। नतीजतन मनुष्य को मौसमी परिवर्तनों मसलन ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस प्रभाव, भूकंप, भारी वर्शा, बाढ़ और सूखा जैसी विपदाओं से जुझना होगा। जलवायु परिवर्तन को लेकर 1972 में स्टाकहोम, 1992 में जेनेरियो, 2002 में जोंहासबर्ग, 2006 में मांट्रियाल और 2007 में बैंकॉक सम्मेलन हुआ। हो रहे बेढ़ब परिवर्तन को लेकर चिंता जतायी गयी। जलवायु को संतुलित बनाए रखने के लिए ढेरों कानून बनाए गए। लेकिन त्रासदी है कि उस पर ईमानदारी से अमल नहीं हुआ। लेक सेक्स सम्मेलन 1949 में इस बात पर बल दिया गया कि प्रकृति के उपकरण एक नैसर्गिक बपौती के रुप में है जिन्हें शीध्रता से नष्ट नहीं करना चाहिए। इसी तरह स्टाकहोम सम्मेलन 1972 में मानवीय पर्यावरण पर घोषणा हुई। सैद्धांतिक रुप से पृथ्वी के प्राकृतिक द्रव्यों जिनमें वायु, पानी, भूमि तथा पेड़-पौधे शामिल हैं, को वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के लिए सावधानीपूर्ण तथा उपयुक्त योजना तथा प्रबंध द्वारा सुरक्षित रखने पर बल दिया गया। 1992 के रिओ शिखर सम्मेलन में कहा गया कि स्थायी विकास के सभी सरोकारों का केंद्र-बिंदु मानव जाति ही है और उसे प्रकृति के साथ पूर्ण समरसता रखते हुए स्वस्थ एवं उत्पादनशील जीवन जीना चाहिए। लेकिन ये सभी सिद्धांत कागजों तक ही सीमित है। उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। लेकिन गौर करें तो आज भी मनुष्य अपने दुराग्रहों के साथ ही खड़ा है। प्रकृति से उसका खिलवाड़ का तरीका पहले से भी जघन्य हो गया है। नतीजा सामने है। प्रकृति भी प्रतिक्रियावादी बनती जा रही है। पर विडंबना है कि मानव जाति समझने को तैयार नहीं। किंतु उसे समझना ही होगा कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर वह स्वयं को सुरक्षित नहीं रख सकता।

(लेखक राजनीतिक व सामाजिक विश्लेषक हैं)