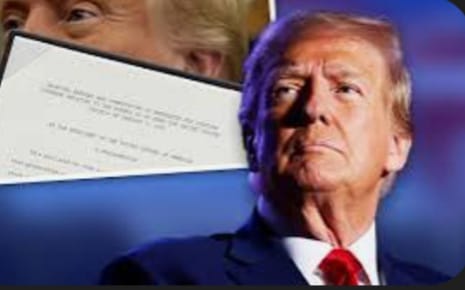लेखक- अमित सिंघल
व्यापार हो या उत्पादन, इनमे टैक्स या टैरिफ के सन्दर्भ में बराबरी (reciprocity) सुनने में न्यायोचित लगता है, लेकिन व्यवहार में नहीं चलता।
उदाहरण के लिए, क्या भारत के दाम वाली चाय या कॉफी अमेरिका में भी मिलनी चाहिए? या फिर, अमेरिका में भारत के समकक्ष वाली मजूरी मिलनी चाहिए, जो प्रतिदिन 1.2 डॉलर या उससे कम बैठेगी।
फिर आप अमेरिकी फेसबुक, गूगल, व्हाट्सएप, एक्स, इत्यादि जैसी “फ्री” सेवाओं का टैरिफ कैसे निर्धारित करेंगे?
अमेरिकी डॉलर में व्यापार करना, लोन लेना, या अमेरिकी शेयर बाजार का चढ़ना-गिरना अन्य देशो पर एक तरह का टैरिफ है। क्योकि अमेरिका नीतिगत हस्तक्षेप से डॉलर के मूल्य को प्रभावित कर सकता है। वर्ष 2008 में कुछ बड़े अमेरिकी बैंको के फेल होने यूरोप की अर्थव्यवस्था डगमगा गयी थी।
सभी यह मानते है कि सभी देश विकास की एक सपाट लाइन में रेस के लिए नहीं खड़े है। हर राष्ट्र के विकास की अपनी एक ट्रैजेक्ट्री है।
टैरिफ, सब्सिडी और व्यापार की बाधाएँ सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये इतिहास को परिलक्षित करते हैं।
उपनिवेशों से अवैध तरीके से दोहन की गयी पूँजी, वहां के उत्पादन को औपनिवेशिक शक्तियों द्वारा अपने क्षुद्र लाभ के लिए ध्वस्त कर देना, अनावश्यक लड़े गए युद्ध, उन युद्धों में किसी एक देश का साथ देना, विकासशील राष्ट्रों में ख़ुफ़िया सेवा द्वारा अस्थिरता को बढ़ावा देना, विकासशील देशो द्वारा विकसित देशो से अधिक ब्याज में लोन लेना, इत्यादि के गर्भ से टैरिफ, सब्सिडी और व्यापार की बाधाएँ निकलती है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अस्तित्व इसके संतुलन में नहीं, बल्कि इसके असंतुलन में है। मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में अमेरिका घाटे या डेफिसिट में रहता है क्योंकि डॉलर विश्व की रिज़र्व मुद्रा है (अर्थात, विश्व के सभी रिज़र्व बैंक अधिकतर विदेशी मुद्रा डॉलर में संचित रखते है), और इसकी मांग सदैव बनी रहती है। अमेरिका माल आयात करने के लिए दूसरे देशों को डॉलर में भुगतान करता है, जो बाद में अमेरिकी संपत्तियों एवं शेयर में निवेश के रूप में वापस आ जाता है।
फिर अमेरिकी डिजिटल गुड्स (गूगल, फेसबुक, एक्स, उबेर, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, कंप्यूटर चिप्स, तकनीकी इत्यादि), मनोरंजन (म्युज़िक, फिल्म, टीवी इत्यादि), एवं अन्य उत्पादों पर पेटेंट का भुगतान (जैसे कि दवाई) इत्यादि पर होने वाले “व्यापार” के कारण अमेरिका अन्य देशो से धन खींचता है और इस “व्यापार” में वह सरप्लस है। इस पर अगर कोई अन्य राष्ट्र टैरिफ लगाने की बात करता है (यूरोपियन यूनियन ने प्रयास किया था), तो उसे अमेरिकी दबाव में वापस लेना पड़ता है।
अमेरिका जैसे विकसित औद्योगिक देश और भारत जैसे कृषि प्रधान देश के बीच व्यापार निष्पक्ष नहीं हो सकता है।
अगर टैरिफ में वास्तव में बराबरी लानी है तो, तो हमें इतिहास को मिटाना होगा। जो असम्भव है। क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की एवं उपनिवेशवाद समाप्त होने के बाद की असमानताओं को इग्नोर करता है।
अमेरिकी नेतृत्व मानता है कि वह एक नए व्यापारिक ओलिंपिक की शुरुवात आज से कर रहा है। यह अमेरिकी उद्यमों के लिए दीर्घकाल में खतरनाक हो सकता है।
हाँ, भारत के सन्दर्भ में संभव है कि भारतीय उद्यमों को उत्पादन के प्रोसेस को और एफिसिएंट करना होगा, उत्पादों को चीन के समकक्ष सस्ता एवं उत्तम गुणवत्ता वाला बनाना होगा। रिसर्च को प्रोत्साहन देना होगा। कृषि को सस्ता बनाना होगा। नहीं तो हम केवल जेनेरिक दवाइयों, हीरो की पोलिश, तेलशोधक इत्यादि के उत्पादक बनकर रह जाएंगे।
संरक्षणवाद मदद करने की जगह कब बैसाखी बन जाता है इसे भारत से अच्छा कौन जान सकता है।
कुछ समय में अमेरिका भी जान जाएगा।
(लेखक रिटायर्ड IRS ऑफिसर हैं)