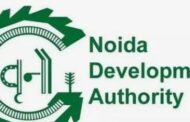लेखक~मुकेश सेठ
भारत में बर्तानिया हुकूमत के विरुद्ध प्रथम क्रान्ति 10 मई को मेरठ में सैनिक विद्रोह और 12 मई को दिल्ली पर कब्ज़े की ख़बर के पश्चात इलाहाबाद में भी प्रारम्भ हुई थी ख़ूनी क्रान्ति
800 नागरिकों को अंग्रेजों ने पेड़ पर लटका दी थी फाँसी,आज 10 मई को प्रथम स्वतंत्रता समर की 166वीं वर्षगाँठ पर ज्ञात-अज्ञात अमर बलिदानियों का सदैव ऋणी रहेगा राष्ट्र
♂÷अखण्ड भारत पर लगभग ढाई सौ वर्षों के क्रूरतम बर्तानिया हुकूमत से माँ भारती की पुण्यभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए लाखों-लाख भारतीयों ने अपना बलिदान दिया तब जाकर देश को ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी से आज़ादी मिली थी।
वर्ष 1857 की मेरठ सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारम्भ प्रथम सशस्त्र क्रान्ति से इसकी ज्वाला देश के अनेक हिस्सों में भी पहुँच गयी थी।
इस विद्रोही क्रांति में हजारों हज़ार विद्रोही क्रांतिकारियों,नागरिकों को अंग्रेजी सत्ता से संघर्ष में वीरगति मिली थी।जिनमें ऐसे भी बलिदानी थे जिनके नेतृत्व में जनता ने अंग्रेजों से 10 दिनों तक हुकूमत छीन कर अपनी सत्ता चलाने में कामयाब रहे थे ऐसे ही एक गुमनाम नायक थे मौलाना लियाकत अली।
समयोचित होगा कि प्रथम सशस्त्र क्रान्ति 10 मई 1857 की ऐतिहासिक संघर्ष की 166 वीं वर्षगांठ पर, एक ऐसे नेता को याद करना सार्थक हो सकता है, जिन्होंने सभी समुदायों और पृष्ठभूमि के पुरुषों और महिलाओं को एकजुट किया।
आज 10 मई 2023 को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 166वीं वर्षगांठ है।
वर्ष 1857 में शुरू हुआ भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम अनिवार्य रूप से मंगल पांडे, नाना साहेब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और वीर कुंवर सिंह जैसी शख्सियतों का पर्याय बन गया।
हालांकि, बड़े पैमाने पर व्यापक आंदोलन होने के कारण, इसके कई नायक गुमनामी में खो गए क्योंकि हम या तो उनके बारे में बहुत कम जानते हैं या कुछ भी नहीं जानते हैं। 1857 के विद्रोह के ऐसे ही एक प्रमुख नेता मौलवी लियाकत अली थे, जो अब के प्रयागराज व तत्कालीन इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे।
मुगल युग के बाद से, इलाहाबाद एक रणनीतिक स्थान रहा है जहां से सम्राट पूरे उत्तर-पश्चिम भारत पर नियंत्रण रखता था। इस कारण बादशाह अकबर ने वहां एक किला बनवाया। यही कारण है कि बाद में अंग्रेजों ने इसे दिल्ली से बंगाल तक फैले क्षेत्र के नियंत्रण केंद्र के रूप में भी बनाए रखा।
विद्रोह के दौरान, मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद में आंदोलन का नेतृत्व किया और 6 जून, 1857 से 16 जून, 1857 तक ब्रिटिश सेना को खदेड़े रखने में कामयाब रहे।
मौलाना लियाक़त अली का जन्म 1810 और 1830 के बीच इलाहाबाद के चैल परगना (अब जिला कौशांबी में) के महगाँव नामक गाँव में एक किसान परिवार में हुआ था। अब रिकॉर्ड के रूप में बहुत कम उपलब्ध है। जब उन्हें 1871 में गिरफ्तार किया गया था, हालांकि, उनकी उम्र 45 साल के रूप में अदालत में दर्ज की गई थी।
उनके पिता का नाम शेख मेहर अली था। उनके चाचा दयाम अली, झांसी में कंपनी बहादुर की सेना में कार्यरत थे । कुछ समय के लिए लियाक़त अली ने अपने चाचा के साथ कंपनी बहादुर के लिए भी काम किया लेकिन उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय सैनिकों के साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार का विरोध किया। इसके चलते उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।
मौलवी लियाकत अली एक प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान थे, और अपने क्षेत्र में उनका बहुत सम्मान भी था। नौकरी से निकाले जाने के बाद वे रास्ते में दिल्ली, भोपाल और टोंक घूमते हुए अपने गांव लौट आए। टोंक में उनकी मुलाकात सैय्यद अहमद शहीदी से हुई, जो तब तक ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ चुके थे।
इसने संभवतः मौलवी को सशस्त्र संघर्ष की ओर धकेला। उन्होंने अपने गांव में एक मदरसा खोला जहां वे बच्चों को पढ़ाते थे। उन्होंने कई जगहों पर तकरीरें भी दिए। इस बीच, उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कंपनी बहादुर और उनके वफादार देशी शासकों के उत्पीड़न के खिलाफ उनके संघर्ष में स्थानीय किसानों को संगठित करना शुरू किया। इलाहाबाद, मिर्जापुर और प्रतापगढ़ में छोटे जमींदारों, तालुकदारों और आम लोगों के बीच वह लोकप्रिय होने लगे वह जल्द ही रोहिलखंड, अवध और कानपुर में एक स्थानीय क्रान्ति नायक के रूप में उभरे।
उनका प्रभाव जल्द ही इलाहाबाद के दारागंज में पांडा समुदाय, कीडगंज और बेनीगंज के प्राग्वाल ब्राह्मणों के साथ-साथ सैदाबाद, रानीमंडी, दरियाबाद, समदाबाद, बेली, नवादा और अन्य जैसे मुस्लिम बहुल गांवों तक फैल गया।
उनके प्रयासों के फलस्वरूप जब 1857 के युद्ध का बिगुल बजाया गया तो इलाहाबाद की जनता सबसे आगे थी।
इलाहाबाद का युद्ध
10 मई को मेरठ में विद्रोह और 12 मई को विद्रोही सेना द्वारा दिल्ली पर कब्जा करने की खबर फैलते ही इलाहाबाद में भी ब्रिटिश सेना सतर्क हो गई।
इलाहाबाद किले के पास उस समय उत्तर पश्चिम भारत में हथियारों और गोला-बारूद का सबसे बड़ा भंडार था। इसकी रक्षा करने के लिए, छठी रेजीमेंट बंगाल नेटिव इन्फैंट्री, जो फिरोजपुर रेजीमेंट का हिस्सा थी, के सिख सैनिकों का एक हिस्सा वहां तैनात था और बाकी कानपुर रोड पर छावनी में थे, जिसमें आमतौर पर ऐसे सैनिक शामिल थे जो भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश के किसान परिवारों से आते थे।
अंग्रेजों ने इलाहाबाद में सेनाएँ भेजनी शुरू कर दीं।
इस बीच, मौलवी लियाकत अली आम लोगों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित कर रहे थे। इलाहाबाद के सभी जमींदारों ने उनके प्रयासों में उनका समर्थन किया तो वहीं सामान्य किसान और शहरी वर्ग भी उनसे जुड़े।
5 जून को खतरे को भांपते हुए ब्रिटिश नागरिकों को किले के अंदर बुलाया गया। गंगा पुल को पार करने वाले विद्रोहियों को रोकने के लिए छठी रेजीमेंट की दो कंपनियों और तीसरे अवध से 150 कैवलरी को अलोपीबाग और दारागंज में लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर के साथ तैनात किया गया था।
इस बीच, लियाकत अली पूरे शहर में बैठकें कर रहे थे और छावनी के साथ-साथ किले के अंदर भी सैनिकों के संपर्क में थे।कहा जाता है कि आठ मेवाती मुस्लिम गांवों की एक बैठक मौजा, शमदाबाद (जहां अब कंपनी गार्डन स्थित है और जहां चंद्रशेखर आजाद 1947 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान शहीद हुए थे) में सैफ खान के घर पर हुई थी। बैठक के मेजबान सैफ खान को छोड़कर, वे सभी उसी दिन संघर्ष में शामिल हो गए।
6 जून की रात 9 बजकर 20 मिनट पर गंगा पुल की रखवाली कर रहे दारागंज में तैनात भारतीय सैनिकों ने विद्रोह शुरू कर दिया। दुर्ग की ओर से आदेश जारी हुआ कि सैनिक अपने हथियार जमा कर दें, लेकिन सैनिकों ने आदेश की अवहेलना करते हुए अपनी बंदूकों के साथ छावनी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया।
लेफ्टिनेंट हार्वर्ड, जो इस बटालियन के अधिकारी थे, पास के अलोपीबाग में तैनात लेफ्टिनेंट अलेक्जेंडर के पास पहुंचे जिन्होंने अपने घुड़सवारों को विद्रोही सैनिकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। इन सिपाहियों ने भी नहीं मानी। जब सिकंदर ने गोलियां चलाईं तो सैनिकों ने उसे मार डाला।
लेफ्टिनेंट हार्वर्ड किसी तरह बच निकलने में सफल रहा और किले तक पहुंच गया। रात 10 बजे, भारतीय सैनिकों ने शहर में सभी अंग्रेजों को मार डाला और खजाना लूट लिया। अगली सुबह सिपाही रामचंद्र के नेतृत्व में 3,000 कैदियों को जेल से मुक्त कराया गया।
7 जून को मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद को स्वतंत्र घोषित कर ऐतिहासिक खुसरो बाग को अपना मुख्यालय बनाया। दो दिन से चली आ रही अराजकता को नियंत्रित करने के लिए मौलवी लियाकत अली ने सिपाहियों और तमाम बागियों के साथ शहर में कूच किया, भाषण दिए और शहर कोतवाली के ऊपर बादशाह का झंडा फहराया।
8 जून को,दिल्ली के बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने मौलवी लियाकत अली को इलाहाबाद के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने के लिए एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए, जो अभी भी हैदराबाद के सालारजंग संग्रहालय में संरक्षित है। उसी दिन मौलवी ने शहर के मामलों के प्रबंधन के लिए एक परिषद और अधिकारियों की नियुक्ति की। शेख नेमत अशरफ को कोतवाल बनाया गया और सुख राय को तहसीलदार नियुक्त किया गया।
पदाधिकारियों को दोनों समुदायों से चुना गया और संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए एक विशाल परिषद की स्थापना की गई। इलाहाबाद के भरवारी रेलवे स्टेशन पर 7 जून को पहले ही कब्जा कर लिया गया था। इसलिए अंग्रेज रेल द्वारा कुमुक तक नहीं पहुँच सके तब इलाहाबाद तक कोई लाइन नहीं थी। तब तक रेलकर्मी भी आंदोलन में शामिल हो चुके थे।
मौलवी को सभी समुदायों का समर्थन प्राप्त था। शहरवासियों से लेकर दोआब क्षेत्र के किसान और गंगा-यमुना के बीच और उससे आगे तक फैले क्षेत्र के छोटे भूमि मालिक उनके साथ थे।
हालाँकि, उस समय की बड़ी रियासतें, जैसे राजा मंडा, राजा दहियाबारा और राजा करछना ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिसके लिए उन्हें बाद में ब्रिटिश हुकूमत ने पुरस्कृत किया था।
उस समय मौलवी लियाकत अली द्वारा जारी किए गए फरमानों से पता चलता है कि वह गहरी समझ वाले और समग्र रूप से प्रतिभाशाली सेनापति थे।
“मुल्क बादशाह का, हुक्म मौलवी लियाकत अली का” (‘सम्राट का देश, मौलवी लियाकत अली का शासन’) उनका आदर्श वाक्य था।
उनके कई आदेश, जैसे एंग्लो-इंडियन पर हमले पर प्रतिबंध लगाना और दुकानदारों से बिना भुगतान के सामान न लेना असाधारण रूप से मानवीय थे।
10 जून तक, मौलवी और उसके लोगों ने किले पर कब्जा करने के प्रयास शुरू कर दिए। कर्नल नील 11 जून को गंगा के दूसरे किनारे से इलाहाबाद पहुंचे। उसके साथ एक विशाल सेना थी। मौलवी को किले के अंदर तैनात सिख रेजीमेंट के 400 सैनिकों से समर्थन मिलने की उम्मीद थी, लेकिन वे अंत तक अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे।
मौलवी ने अकबर द्वारा निर्मित जामा मस्जिद पर एक पुरानी तोप राइफल रखकर किले में घुसने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। किले की चाबियां शहर के एक प्रसिद्ध खत्री परिवार के पास थीं जिन्होंने उन्हें मौलवी को सौंपने का वादा किया था लेकिन जब मौलवी के दो आदमी उनसे मिलने आए तो परिवार ने उन्हें धोखा दिया और उन दोनों को अंग्रेजों ने मार डाला।
अंत में 15 जून को किले के बाहर मौलवी की सेना और अंग्रेजों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। मौलवी के पास अधिक सैनिक थे, फिर भी उसे पीछे हटना पड़ा क्योंकि उसके हथियार पुराने थे और उसकी सेना कम प्रशिक्षित थी उसके कई सैनिक घायल या मारे गए।
मौलवी खुसरो बाग लौट आये। 16 जून को कर्नल नील की सेना ने खुसरो बाग की घेराबंदी की और आक्रमण शुरू कर दिया। शाम तक, मौलवी को चेतावनी दी गई कि अगर उसके लोगों ने हथियार नहीं डाले तो पूरे शहर में आग लगा दी जाएगी।
अन्ततः 17 जून को कर्नल नील और उसकी सेना को चकमा देकर मौलवी अपने 3000 साथियों सहित कानपुर की ओर निकल पड़े और नाना साहब से मिले।
18 जून को, समदाबाद सहित मेवाती मुसलमानों के आस-पास के आठ गाँवों को जला दिया गया और जिसने भी भागने की कोशिश की उसे गोली मार दी गई।
बाद में, सभी सरकारी भवनों, उच्च न्यायालय, सभी पुलिस मुख्यालयों, अटॉर्नी जनरल के कार्यालय के साथ-साथ सिविल लाइंस का निर्माण अंग्रेजों द्वारा इन गांवों के अवशेषों पर किया गया था। इस विद्रोह में इलाहाबाद शहर के लगभग 6,000 लोग मारे गए थे।
ब्रिटिश सेना ने कोतवाली, कीडगंज, दारागंज, बेनीगंज, दरियाबाद और सैदाबाद के आस-पास के इलाकों में भयानक नरसंहार किया। अभिलेखों के अनुसार चौक पर करीब 600 से 800 लोगों को नीम के पेड़ पर लटकाया गया था।
‘फाँसी इमली’ का पेड़” नरसंहार का गवाह इमली का पेड़ आज भी कानपुर रोड पर खड़ा है। इसके बावजूद मौलवी ने लड़ना नहीं छोड़ा। 1858 तक गंगा के उस पार के इलाके पर मौलवी की सेना का कब्जा था। 1858 में मौलवी ने अपनी आखिरी लड़ाई मेजर बर्कले के खिलाफ लड़ी, वह इसमें भी बच गए।
विद्रोह की विफलता के बाद, मौलवी गुजरात में सूरत के पास लाजपुर में हकीम अब्दुल करीम के रूप में प्रच्छन्न होकर भूमिगत रहे और बाद में बंबई चले गए। यहां वह एक व्यापारी बाकिर अली के घर ठहरे। जब वह एक मस्जिद में तक़रीर दे रहे थे, तो स्रोताओं में से दो लोगों ने उन्हें पहचान लिया और ब्रिटिश अधिकारियों को सूचित किया।
उन्हें 7 जुलाई, 1871 को बंबई के बायकुला स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था, इस घटना की ख़बर न्यूयॉर्क टाइम्स,टाइम्स लंदन और सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी।
मौलाना लियाकत अली एक साल जेल में रहने के बाद 18 जुलाई, 1872 को इलाहाबाद में न्यायाधीश एआर पोलक की अदालत में उनका मुकदमा शुरू हुआ। जज पोलक ने लिखा है कि सुनवाई के दौरान मौलवी के लाखों समर्थक उनकी एक झलक पाने के लिए कोर्ट के बाहर जमा हो गए।
उसके पकड़े जाने और मुकदमे की खबर सुनकर, कानपुर विद्रोह से बचने वाली एकमात्र अंग्रेज महिला एमी हार्नी, जो तब 17 साल की थी, मौलवी के पक्ष में गवाही देने के लिए इलाहाबाद पहुँची। अपने बयान में, उसने गवाही दी कि मौलवी ने न केवल उसकी जान बचाई बल्कि उसे उसके परिवार के साथ सुरक्षित रूप से फिर से मिला दिया। हार्नी, सबिहा व्हाइट, और कई अन्य महिलाओं की गवाही सुनने के बाद, न्यायाधीश पोलक ने मौलवी की मौत की सजा को “कालापानी” की सजा में बदलकर उन्हें पोर्ट ब्लेयर भेज दिया गया।
मौलवी ने 1892 में अंतिम सांस ली। इलाहाबाद के राजकीय पुस्तकालय में अभी भी उनके मामले की पूरी फाइल है, लेकिन यह फारसी में है, जैसा कि उस समय प्रथा थी, और अब फ़ारसी भाषा के कुछ ही पाठक बचे हैं।
आजादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू 1957 में मौलवी के वंशजों से मिले थे। उनकी तलवार और फटा कुर्ता-पायजामा इलाहाबाद संग्रहालय में संरक्षित है। उनके वंशज महगाँव और करेली के कुछ इलाकों में बसे हैं। स्थानीय ग्रामीणों और उनके परिवार के प्रयासों से करेली में एक शैक्षणिक संस्थान, एक पुस्तकालय उनके नाम पर खोला गया।
जिस देश में हर दूसरे दिन शहरों और सड़कों का नामकरण और नामकरण किया जाता है और हर नुक्कड़ पर मूर्तियाँ स्थापित की जाती हैं, मौलवी की स्मृति में ऐसा कोई सम्मान नहीं दिया गया है।
आज जब साम्प्रदायिक राजनीति और नफरत का बोलबाला है, तो इस गुमनाम नायक को याद करना सार्थक है।
स्वतंत्र भारत की सरकारें भले ही अपने वीरों की स्मृति का सम्मान करने में विफल रही हों, लोगों ने उन्हें अपने गीतों और लोकगीतों में जीवित रखा है।
बहादुर शाह जफर द्वारा अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए एक दोहा याद आता है, जो उनके समय के सभी शहीदों के लिए समान रूप से उपयुक्त है:
तेरी किस्मत कैसी बदनसीब है जफर! कि तेरी श्मशान भूमि के रूप में
दो गज की दूरी भी प्रियतम की भूमि में न हो।

÷लेखक स्वतन्त्र पत्रकार हैं÷